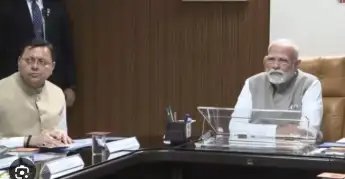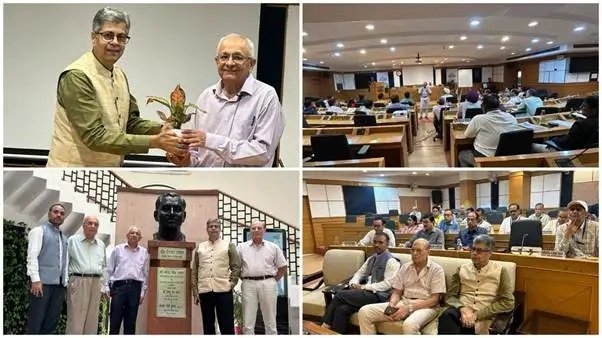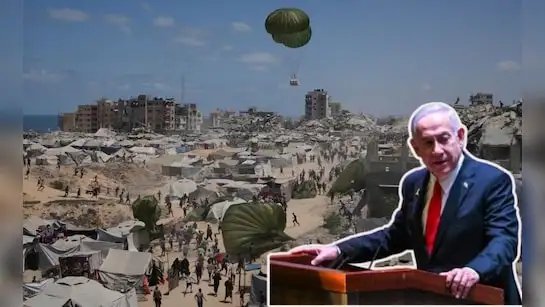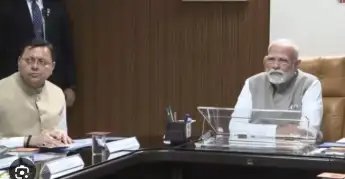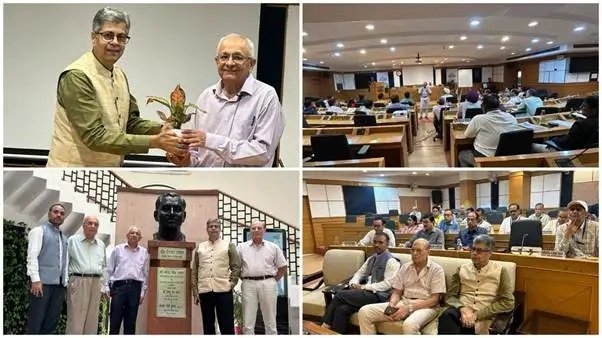बाजरा भारत की प्राचीन और प्रमुख अनाज फसलों में से एक है। इसे लंबे समय से गरीबों का भोजन कहा जाता रहा है, लेकिन आज के समय में इसके पोषण मूल्य के कारण यह अमीरों की डाइट का हिस्सा बन गया है। बाजरा शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, आयरन, प्रोटीन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है। यही कारण है कि आज विश्व स्तर पर भी इसकी मांग बढ़ रही है और इसे सुपरफूड के रूप में पहचान मिल रही है।
बाजरे की किस्में और उपयुक्त क्षेत्र
भारत में बाजरे की कई किस्में उगाई जाती हैं। देसी किस्में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल होती हैं, जबकि उन्नत किस्में जैसे HHB-67, ICTP-8203 और ICMH-356 अधिक उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधक होती हैं। बाजरे की खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए आदर्श हैं। मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट या हल्की मिट्टी सबसे बेहतर परिणाम देती है।
भूमि की तैयारी और बुवाई का समय
बाजरे की खेती शुरू करने से पहले खेत की 2-3 बार गहरी जुताई करना जरूरी होता है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और बीज अच्छे से अंकुरित हो सकें। खेत में यदि गोबर की सड़ी हुई खाद डाली जाए तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। खरीफ सीजन में इसकी बुवाई का सही समय जून से जुलाई तक माना जाता है। बीजों को बुवाई से पहले फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करने पर पौधे अधिक स्वस्थ और रोग मुक्त रहते हैं। कतारों में बुवाई करना अधिक लाभकारी होता है और पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखने से उत्पादन बेहतर मिलता है।
खाद, उर्वरक और सिंचाई
बाजरे की खेती (Bajre ki Kheti) में जैविक खाद का इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी होता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व सही मात्रा में डालने चाहिए। सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 40-60 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फॉस्फोरस देना पर्याप्त होता है। चूँकि बाजरा वर्षा आधारित फसल है, इसलिए अधिकतर किसान इसे बरसात के पानी पर उगाते हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है, वहाँ दो से तीन सिंचाइयाँ देने पर उपज में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
खरपतवार और रोग नियंत्रण
बाजरे की फसल में खरपतवार तेजी से पनपते हैं, इसलिए समय-समय पर निराई करना जरूरी है। रोगों और कीटों में तना छेदक और माहू प्रमुख हैं, जिनका नियंत्रण जैविक उपायों से किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित रसायनों का भी प्रयोग किया जा सकता है ताकि पैदावार पर असर न पड़े।
कटाई और भंडारण
जब बालियाँ पूरी तरह पक जाती हैं और अनाज सख्त हो जाता है, तब फसल कटाई के लिए तैयार होती है। कटाई के बाद अनाज को अच्छी तरह सुखाना जरूरी होता है ताकि भंडारण के समय नमी के कारण खराब न हो। इसे साफ और हवादार स्थान पर बंद बोरों या डिब्बों में रखना चाहिए।
उत्पादन और लाभ
सामान्य परिस्थितियों में बाजरे की औसत पैदावार 18 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, लेकिन उन्नत किस्में और बेहतर तकनीक अपनाकर यह उत्पादन 30 क्विंटल या उससे अधिक तक पहुँच सकता है। बाजरा न केवल किसानों को बेहतर आमदनी देता है, बल्कि बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। आजकल लोग इसे हेल्दी डाइट के रूप में अपना रहे हैं और इससे बने आटे, कुकीज, ब्रेड और पिज्जा बेस जैसे उत्पाद लोकप्रिय हो रहे हैं।
सरकारी योजनाएँ और भविष्य की संभावनाएँ
भारत सरकार बाजरे को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करती है, जिससे किसानों को सुरक्षित बाजार मिलता है। कई राज्यों में बीज, उर्वरक और सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी भी दी जाती है। आने वाले समय में बाजरे की मांग और बढ़ने की संभावना है क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ता इसे तेजी से अपना रहे हैं। निर्यात के क्षेत्र में भी इसके बड़े अवसर हैं।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर बाजरे की खेती कम लागत में अधिक लाभ देने वाली फसल है। यह सूखे क्षेत्रों में भी आसानी से उगाई जा सकती है और किसानों की आमदनी को स्थायी बनाने में मदद करती है। इसके साथ ही यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अमृत के समान है। यदि किसान उन्नत किस्मों, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करें, तो बाजरे की खेती भविष्य में उनके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।